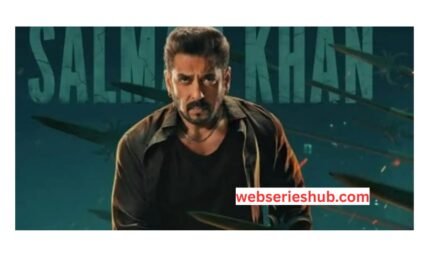Santosh: दो कहानियों की एक फिल्म पहली कहानी इस विचार से शुरू होती है कि ‘संतोष’ – जिसका अर्थ होता है खुशी या संतुष्टि – आमतौर पर पुरुषों का नाम माना जाता है। लेकिन इस फिल्म में, संतोष एक महिला है। 28 साल की विधवा, संतोष सैनी (शहाना गोस्वामी), जिसे अपने दिवंगत पति की पुलिस की नौकरी मिल जाती है। यह काम उसकी जरूरत भी है और चुनौती भी। पुलिस बल, जहां पुरुषों का वर्चस्व है, वहां एक महिला कांस्टेबल की जगह बनाना आसान नहीं। लेकिन उसे एक सशक्त साथी मिलती है – गीता शर्मा (सुनीता राजवार), जो सालों से पुलिस में अपनी पहचान बना चुकी हैं और महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं।
संतोष और गीता एक भयावह केस की जांच में जुटती हैं – एक 15 साल की लड़की के बलात्कार और हत्या का मामला। यह केस संतोष के लिए सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि खुद को साबित करने का मौका भी है। वह अपने सीनियर्स को दिखाती है कि वह सिर्फ ‘दया नियुक्ति’ से आई महिला नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत से पहचान बनाने वाली पुलिसकर्मी है।
See More : Be Happy Movie Review: अभिषेक बच्चन और इनायत वर्मा के साथ एक इमोशनल रोलरकोस्टर राइड
एक फिल्म, दो नजरिए
यह वही फिल्म है, जिस पर कुछ लोग गर्व करेंगे। एक प्रेरणादायक सफर, जिसमें एक महिला मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ती है। यह संघर्ष की कहानी है, जहां एक महिला अपने हक के लिए खड़ी होती है और पितृसत्ता को चुनौती देती है। संतोष खुद इस पर विश्वास करती है। यह उसकी दुनिया के खिलाफ जंग है।
लेकिन यह वही फिल्म भी है, जो समाज को एक सपने की तरह दिखाई जाती है – एक सीधी, स्पष्ट और आसान कहानी, जहां सवाल कम और जवाब ज्यादा होते हैं। इसमें जटिलता नहीं, सच्चाई नहीं, और न ही असल जिंदगी की उलझनें। यह फिल्म वैसी दुनिया दिखाती है, जिसे लोग देखना चाहते हैं – जहां हर चीज साफ-सुथरी, सीधी और आसान हो। क्योंकि कभी-कभी, अज्ञानता ही असली ‘संतोष’ होती है।
दूसरी फिल्म: परछाइयों की कहानी
यह कहानी उन चमकते हैशटैग्स और सीधी-सपाट कहानियों के पीछे छिपी सच्चाई की है। यह एक ऐसी फिल्म है, जो असहज करती है, सवाल खड़े करती है—और जिसे वही समाज अनदेखा कर देता है। लेकिन कांस्टेबल संतोष सैनी इसी कड़वी हकीकत में खुद को पाती है।
यह संतोष एक और संघर्ष की तस्वीर है। एक विधवा, जो घुटन से निकलने के लिए इतनी बेताब है कि अनजाने में वही बन जाती है, जिससे वह बचना चाहती थी। पहली बार वह बिना किसी सहारे दुनिया से टकराती है, और जो उसे दिखाया जाता है, वही उसकी सच्चाई बन जाती है। उसे जो कहानी दी जाती है, वह उसी पर भरोसा कर लेती है।
संतोष: परतों के पीछे की कहानी
चिराग प्रदेश—जहां नफरत धधकती है, जाति जंजीर बनती है, और कानून मौन रहता है। शहर मेहरत, जो मेरठ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं।
15 साल की दलित लड़की मारी जाती है। पुलिस बहरी बनी रहती है, जब तक कैमरे नहीं चमकते। नेता चाहते हैं कि मामला जल्दी पटाक्षेप हो—सिर्फ दिखावे के लिए।
गीता शर्मा आती हैं। वो दबाव में केस निपटाने की विशेषज्ञ हैं। संतोष उनके प्रभाव में बहने लगती है। संदिग्ध चुना जाता है—सलीम। चंद टेक्स्ट मैसेज ही उसके अपराधी होने का सबूत मान लिए जाते हैं।
जांच वहां पहुंचती है, जहां संतोष का पति रमन दंगों में मारा गया था। गीता चाहती हैं कि सलीम को सबक बनाया जाए। संतोष सहमत होती है—फिर धीरे-धीरे उसे दिखता है कि वो खुद भी एक खेल का मोहरा बन चुकी है।
कानून लागू करने की जगह, वो सोच लागू कर रही थी।
वो दो तरह के ‘अछूतों’ के बीच खड़ी थी—एक वे, जिन्हें समाज छूना नहीं चाहता। और दूसरे वे, जिन्हें कोई छू नहीं सकता।
संध्या सूरी की दुनिया
संध्या सूरी एक ऐसा माहौल गढ़ती हैं, जहां समाज की चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। यह भारतीय संदर्भ में स्क्विड गेम जैसी सत्ता-चालित चालबाजी या अनोरा जैसी त्रासद व्यंग्य-कथा है।
संतोष की दुनिया में शीर्ष पर बैठे पुरुष सत्ता को बनाए रखने के लिए जाति, वर्ग, धर्म और लिंग को आपस में भिड़ा देते हैं। गीता शर्मा, एक भ्रष्ट और उच्च जाति की अधिकारी, इस शोषण का गर्वित हिस्सा बन जाती है। संतोष को यह यकीन दिलाया जाता है कि उसे अपनी जगह बनाने के लिए इस खेल का हिस्सा बनना ही होगा।
उसकी बेबाकी को हथियार बना दिया जाता है। अंधी बहादुरी और महत्वाकांक्षा का शोषण होता है। सवाल न पूछने का इनाम?—बनोफी पाई।
वह एक “ध्यान भटकाने वाली कहानी” बन जाती है। फॉर्मूला सीधा है—कठिन सवालों का सामना मत करो, बस “महिला सशक्तिकरण” का नारा लगा दो। लोग बस यही देखेंगे कि एक विधवा पुरुषों को सजा दे रही है और ऊपर बढ़ रही है—यह नहीं कि वह आखिर कहां जा रही है।
फिल्म का एक बेहतरीन दृश्य—एक कार में
कार में गीता शर्मा का अंदाज सख्त है—सिगरेट के धुएं के साथ अनुभव की बातें, गाड़ी के पहियों के संग सत्ता का एहसास, बैकग्राउंड में पुराने बॉलीवुड गाने। वह सिनेमा और हकीकत के खेल को जोड़ती है—कहती है, “हर कोई अभिनय करता है”। पूछताछ में मुसलमान ‘पीड़ित’ बनने का नाटक करते हैं, और वह झूठ गढ़कर उन्हें डराती है।
संतोष सुनती है, मोहित होकर, सिर हिलाते हुए। वह इस सुपरवुमन के जादू में बंध चुकी है।
यह दृश्य आज के सिनेमा और उसके दर्शकों का आईना है—जहां नफरत को ‘सशक्तिकरण’ और ‘संस्कृति की रक्षा’ का नाम देकर परोसा जाता है, और दर्शक उसे सच मानकर आत्मसात कर लेते हैं।
दिलचस्प है कि सुनीता राजवार, जिन्हें अक्सर छोटे, हास्यपूर्ण किरदारों तक सीमित कर दिया जाता है, यहां खुद एक झूठी कथा की प्रतीक हैं। गीता, कहानियां नहीं कहती, उन्हें मिटाती है।
वहीं, शहाना गोस्वामी की संतोष वह दर्शक बन जाती है जो इस भ्रम को सच मान लेती है।
संतोष ने पत्नी, बेटी, बहू के किरदार इतने लंबे समय तक निभाए कि अब वह सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर रह गई है।
वह भेदभाव को देखती है—शायद आंकती भी है। जब पुलिस ‘शुद्धिकरण’ करती है, जब शव को ले जाने से लोग इनकार करते हैं, वह प्रतिक्रिया की उम्मीद करती है, मगर सब चुप हैं।
शुरुआत में लगता है कि संतोष ‘मुख्य किरदार’ होने के चलते स्वाभाविक रूप से सही और अलग होगी।
लेकिन उसके पूर्व ससुराल वाले उसे ‘बागी’ और ‘अपशकुनी’ कहते हैं—मानो उसने हमेशा अपने ढंग से चलने की कोशिश की हो, भले ही ऊपर से वह आज्ञाकारी दिखती रही हो।
संतोष के लिए उसका ज़मीर उसकी पहचान से छोटा पड़ जाता है। वह जज नहीं कर रही, बस देख रही है, सीख रही है, ढल रही है।
शुरुआती दृश्यों में, जब वह एक सीनियर कांस्टेबल के साथ गश्त पर निकलती है, तो जोड़ों को पकड़ते वक्त वह पहली बार ताकत का नशा महसूस करती है। उस वक्त, उसे मजहब नहीं दिखता, बस औरतों के प्रति समाज की हुकूमत दिखती है।
फिल्म छोटे-छोटे लम्हों में उसके मन के बदलाव के बीज बोती है।
उसके दो अफसर मानते हैं कि उसके पति की मौत किसी मुस्लिम दंगाई ने की थी—यह बात धीरे-धीरे उसके अंदर घर करने लगती है।
एक सीन में, पुलिस वैन के भीतर, गीता उसके करीब झुकती है—एक पल को मानो वह किसी और इरादे से आई हो।
लेकिन नहीं—वह संतोष की नाक में नथ पहनाती है। जैसे याद दिला रही हो कि वह एक योद्धा तो बन सकती है, लेकिन एक तय दायरे में ही।
यह बदलाव दिखता नहीं, बस महसूस होता है।
संतोष एक मुस्लिम इलाके में निगरानी के दौरान खाने बैठती है। वह देखती है—एक आदमी घूर रहा है। गोस्वामी की देहभाषा बता देती है—अब घूरती नजरें उसके लिए सिर्फ नजरें नहीं, बल्कि एक पहचान बन चुकी हैं।
बाद में, जब वह एक संदिग्ध को पीटती है, तो ऐसा लगता है जैसे उसने भीतर दबा गुस्सा और दुनिया का दबाव निकाल दिया हो। उसे बस किसी को दोष देना है—एक धर्म, एक इलाका, एक नाम—अपने पति की मौत के लिए, अपने खत्म हुए सपनों के लिए।
वह सिर्फ एक पत्नी थी। उसे रोने तक का हक़ नहीं मिला। बस एक रात का सन्नाटा, एक कमीज़ की हल्की खुशबू। उसने खून से सनी वर्दी धो दी, आंसू पोंछे, और चुपचाप अंगूठी उतार दी। यादें भी उसके लिए एक लग्ज़री थीं।
गोस्वामी की अदाकारी इस दुःख को भ्रम की चमकदार परत पहना देती है। यह उसे एक झूठा लक्ष्य, एक झूठी ताकत देता है। क्योंकि सबसे आसान चीज़ यही है—एक जख्म को खुला छोड़ दो, तो वह जहर बन जाता है।
फिल्म का एक दृश्य—संतोष रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। दूसरे प्लेटफॉर्म पर एक जोड़ा। बीच में गुजरती ट्रेन।
झलकियों में दिखता प्यार—कभी पूरा, कभी अधूरा। जैसे कोई बिखरा हुआ ऐनिमेटेड सीन।
लेकिन यह सिर्फ एक दृश्य नहीं, एक हकीकत है।
एक देश, जो दो प्लेटफॉर्म्स के बीच अटका है।
जहां प्यार ठहरता नहीं—धीरे-धीरे, खो जाता है।